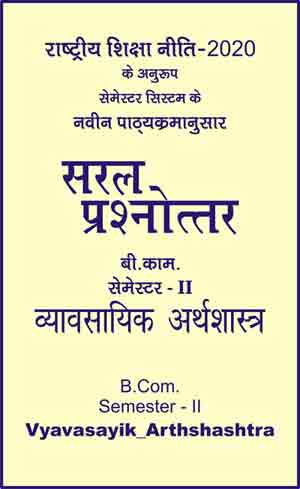|
बी काम - एम काम >> बीकाम सेमेस्टर-2 व्यावसायिक अर्थशास्त्र बीकाम सेमेस्टर-2 व्यावसायिक अर्थशास्त्रसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीकाम सेमेस्टर-2 व्यावसायिक अर्थशास्त्र - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 11 - पैमाने के प्रतिफल, आन्तरिक व बाह्य मितव्ययिताएँ तथा अमितव्ययिताएँ
(Returns to Scale, Internal and External Economies and Diseconomies)
पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बताती है। दीर्घकाल में सभी उत्पादन के साधन बदले जा सकते हैं। उत्पादन तकनीकी में सुधार, श्रम विभाजन एवं विशेषज्ञीकरण आदि के कारण उत्पादन में आन्तरिक एवं बाह्य बचत उत्पन्न होती है, किन्तु यह बचत स्थायी नहीं रह पाती और बाद में हानियों के रूप में बदलने लगती है।
पैमाने के प्रतिफल के अन्तर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी साधनों का विस्तार किया जाए तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पैमाने के प्रतिफल स्थिर भी हो सकते हैं, बढ़ते या अथवा घटमान भी। चेचर्सल तथा अन्य मत है कि जब उत्पादक के सभी साधनों की मात्रा बढ़ायी जाती है तो उत्पादन के पैमाने बढ़ जाते हैं। साधनों की अधिक मात्रा में उपयोग से विशेषज्ञीकरण, समानता तथा अप्रत्याशित रूपान्तरण साधनों, विशेष रूप से उत्तम मशीनों के प्रयोग की सुविधा, उत्पादन के पैमाने में वृद्धि के कारण उत्पादन विशेष पर कम लागत की उपलब्धता, अधोसंरचना का विकास, उत्पादन में होने वाले बेस्ट के प्रयोग से उप-उत्पाद विकसित होने के कारण लागत में कमी दृष्टिगोचर होती है। इसे मितव्ययिता या किफायती कहते हैं।
मितव्ययिता की प्रक्रिया के प्रतिफल का श्रेय मार्शल को है। प्रबन्ध तथा सम्पर्क की कमी, अत्यधिक मशक्कत तथा उत्पादन क्रिया की जटिलता के कारण उत्पादन लागत बढ़ने लगती है। इसे उत्पादन की अमितव्ययिता कहते हैं।
यदि सभी साधनों को एक विशेष अनुपात में बढ़ाया जाए और परिणाम स्वरूप उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़े तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होंगे। यदि सभी साधनों को दुगुना करने से उत्पादन भी दोगुना हो जाता है तो पैमाने के प्रतिफल स्थिर होंगे। परन्तु यदि सभी साधनों को बढ़ाने से उत्पादन में अधिक अनुपात से वृद्धि होती है तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होंगे।
किसी कारखाने या फर्म के अच्छे प्रबन्ध या विस्तार में प्रकट होने वाली बचतें आन्तरिक बचतें कही जाती हैं ये बचतें आन्तरिक प्रवृत्त का परिणाम होती हैं। आन्तरिक बचतों के प्रकार इस प्रकार हैं -
श्रृंखला-विक्रय से होने वाली बचतें, नई एवं विशिष्ट मशीनों के उपयोग से बचतें, श्रम-विभाजन के उपयोग से बचतें, अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग, विज्ञापन एवं विक्रय कला में बचतें, शत्रु व्यवसाय में बचतें, पैकेजिंग से होने वाली बचतें, कम ब्याज दर ऋण, प्रयोग व शोध, कुशल व योग्य संगठनकर्त्ताओं की सेवाओं से बचतें आदि।
उद्योगों के विस्तार होने पर बाह्य बचतों की उत्पत्ति होती है। ये बचतें किसी विशेष फर्म के बारे में न होकर सभी फर्मों में समान रूप से मिलती हैं। बाह्य बचतों के प्रकारों में तकनीकी बचतें, विशिष्टता की बचतें, तकनीकी ज्ञान की बचतें आदि आती हैं।
जब उद्योगों का अधिक विस्तार हो जाये तो पूँजी की प्राप्ति में कठिनाइयाँ, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या का ज्यादा होना, उत्पादन की बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाना आदि तत्व शामिल हैं। बड़े पैमाने के उत्पादन की कई हानियाँ जैसे - औद्योगिक संघर्ष, कारखाना प्रणाली के दोष, लघु उद्योगों का पतन, धन का असमान वितरण, व्यक्तिगत रुचि की उपेक्षाल, एकाधिकारी प्रवृत्ति, मशीनों के उपयोग की हानियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष, श्रम-विभाजन की हानियाँ आदि हैं।
|
|||||