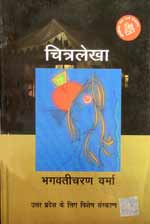|
बी ए - एम ए >> चित्रलेखा चित्रलेखाभगवती चरण वर्मा
|
|
||||||
बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक
3
विद्या, ज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शिक्षा
(Vidya, Gyan, Teaching, Training and Education)
प्रश्न- शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में प्रकाश डालिए।
उत्तर-
शिक्षा का कार्यकारी पहलू शिक्षण है जिसे वह स्वयं नहीं बल्कि दूसरों की सहायता (शिक्षक) से प्राप्त करता है। शिक्षण का लक्ष्य ज्ञान, अनुभव, कौशल प्रदान करना होता है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक और विद्यार्थी के परस्पर आपसी विचार-विनिमय या अन्तःक्रिया द्वारा संचालित होती है। अतएव- कहा जा सकता है कि - "शिक्षण शिक्षक की सप्रयोजन, सचेतन, लक्ष्यपूर्ति से सम्बन्धित तकनीकी (विधि) है जिसका सम्बन्ध विषय-वस्तु को शिक्षार्थियों को आत्मसात् कराने की प्रक्रिया से होता है।'
शिक्षण की अवधारणा को अनेक शिक्षाविद अलग-अलग दृष्टिकोण से प्रकट करते हैं। शिक्षाविदों के दृष्टिकोणों को निम्नवत् समझा जा सकता है -
शिक्षण की संकुचित अवधारणा
(Narrower Concept of Teaching)
(1) शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है (Teaching is a Bipolar Process) - एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। उनका मानना है कि शिक्षण के दो मुख शिक्षक और शिक्षार्थी हैं शिक्षक अपने व्यक्तित्व से शिक्षार्थी के विकास हेतु व्यवहार को परिवर्तित करता है इस प्रकार शिक्षण की यह प्रक्रिया एक चेतन और विचारपूर्ण प्रक्रिया है।
(2) शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है (Teaching is a Tripolar Process) - जॉन डीवी शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं उनका मानना है कि शिक्षक और शिष्य के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व भी है। यह तत्व विषय-वस्तु हैं। शिक्षण की प्रक्रिया इन तीन केन्द्र बिन्दुओं के आपसी सम्मिलन से गतिशील होती है। इन तीनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में शिक्षण की प्रक्रिया अस्त-व्यस्त सी हो जाती है। अतः शिक्षण तीन सामूहिक पक्षों के सम्मिलन पर आधारित अन्तः क्रियात्मक प्रक्रिया है।
(3) शिक्षण एक कला है (Teaching is an Art) - एमीडोन के मतानुसार "जिस प्रकार शिल्प का संगमरमर के टुकड़े से सम्बन्ध होता है ठीक उसी प्रकार से शिक्षण का सम्बन्ध मानव आत्मा से होता है जिससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार कलाकार कलात्मक दक्षता को प्रकट करता है ठीक उसी प्रकार शिक्षक अपनी शिक्षण कला से शिक्षार्थी की आत्मा में निहित ज्ञान को बाहर निकालकर उसे नवीन रूप देता है।
(4) शिक्षण विज्ञान है (Teaching in a Science) - सिल्वरमैन का मानना है कि शिक्षण विज्ञान है। उन्होंने लिखा है कि "यदि विश्वासपूर्वक कहा जाए कि शिक्षण औषधियों का अभ्यास करने जैसी कला है वही अगर इसे दूसरे तरीके से कहें तो उसे बुद्धि उत्पन्न करने की शक्ति का अभ्यास कहा जा सकता है। परन्तु उसमें औषधियों जैसा कि विज्ञान भी है क्योंकि उसे तरीकों, तकनीकों तथा कौशलों को एकत्र करने की आवश्यकता होती हैं। जिससे कि अध्ययन वर्णन और परिमार्जन सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकें। एक उत्तम शिक्षक, एक निपुण चिकित्सक की तरह होता है जो कि मूलभूत संग्रह को सृजनशीलता एवं प्रेरणा प्रदान करके समृद्धशाली बनाता है।
(5) शिक्षण बालक का व्यवहार परिवर्तन है (Teaching is a Change of Pupil's Behaviour) - क्लार्क के अनुसार, “शिक्षण वह क्रिया है जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं संचलित की जाती है।' गेज के अनुसार, “शिक्षण अन्तः वैयक्तिक प्रभावों का स्वरूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार विभव को परिवर्तित करना है।'
उपरोक्त मतों के अनुसार यह स्पष्ट है कि शिक्षण की अवधारणा विविधता से युक्त है। ये सभी दिए गए दृष्टिकोण शिक्षण के एकांगी पक्ष को प्रकट करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षण एकांगी न होकर बहुआयामी दृष्टिकोण से समन्वित है।
(6) शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान है (Teaching is Problem Solving) - जॉन ब्रूवेकर के मतानुसार, "सीखने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके सीखने की ओर अभिप्रेरित करना शिक्षण है।'
शिक्षण की व्यापक अवधारणा
(Wider-Concept of Teaching)
शिक्षण की व्यापक अवधारणा की बात की जाए तो शिक्षण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्वरूप और शासन व्यवस्था आधारित दृष्टिकोण से कुछ विद्वानों ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देश की शिक्षण प्रणाली देश में निहित राजनैतिक व्यवस्था तथा शासन पद्धति से काफी प्रभावित होती है। शिक्षण का स्वरूप एकतंत्रीय शासन व्यवस्था में कठोर, स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विकास का दमन करने वाला होता है जबकि जनतन्त्रीय शासन में शिक्षण सरल, नमनीय, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से आच्छादित तथा बालकों के विकास को मूर्तरूप देने वाला होता है।
एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ
(Meaning of Teaching in Autocratic Gov.)
एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षण का स्वरूप शासक के आदेशों पर आधारित होता है. शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी इच्छा से शिक्षण के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, पूरी शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक केन्द्रित होती है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, इच्छा, आवश्यकता, अभिरुचि, योग्यता को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। शिक्षण में मनोविज्ञान का पूरी तरह से लोप रहता है। शिक्षार्थियों के मौलिक क्षमता को विकसित नहीं होने दिया जाता। इसमें स्मृति को बढ़ाने वाले ही प्रकरणों को पढ़ाया जाता है। बालक की मनोभावनाओं और जीवन-दर्शन को पूरी तरह दमित रखने का प्रयास इसके शिक्षण में किया जाता है।
जनतन्त्रीय शासन-व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ
(Meaning of Teaching in Democracy)
इसके अन्तर्गत शिक्षण का स्वरूप मनोवैज्ञानिक पहलुओं से आच्छादित तथा शिक्षण-शिक्षार्थी सम्बन्ध को मानवीय गरिमा से सम्युक्त होता है इसमें शिक्षक-शिक्षार्थी अपने मनोनुकूल शिक्षण में सहभागी हो सकते हैं। इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया को बाल-केन्द्रित बनाने पर बल दिया जाता है।
शिक्षण-प्रतिरूप या प्रकारताएँ
(Modalities of Teaching)
आधुनिक विचारधारकों ने चिन्तन-मनन के द्वारा और शोध के द्वारा शिक्षण के नवीन कलेवर देने में विशेष रुचि लिया। आज शिक्षण में नये-नये आयामों को अपनाया जा रहा है। शिक्षण को मापनीय बनाने पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इसमें शिक्षण प्रतिरूप के अन्तर्गत अनुबन्धन प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा प्रतिपादन को स्थानापन्न किया गया है।
प्रायः ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक शिक्षक की यह प्रबल कामना होती है कि उसका शिक्षण विद्यार्थियों के अनुकूल हो, उन्हें जो भी सूचना दी जा रही है वह उसे ठीक से समझ सकें। शिक्षक की इस अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए शिक्षण में कुछ नवीन शब्दावलियों को स्थापित करते हुए शिक्षण के समानार्थी के रूप में महत्व कतिपय विद्वानों द्वारा दिया गया है। मुख्य रूप से शिक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना तथा कौशलों का विकास करना है।
शिक्षण और प्रशिक्षण
(Teaching & Training)
शिक्षण बहुआयामी पक्षों के विकास से सम्बन्धित होता है। शिक्षण से शिक्षार्थी में 'ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है। शिक्षण को शिक्षक के माध्यम से तब तक दिया जाता है जब तक शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, सुधार अथवा नवीन ज्ञान का आत्मसातीकरण नहीं हो जाता। शिक्षण से छात्रों में विश्वासों तथा दृष्टिकोणों में नवीनता का संचार होता है। अतः शिक्षण का मूलाधार व्यवहार परिवर्तन को मूर्त रूप देना और ज्ञान का प्रसारण है।
शिक्षण के सापेक्ष प्रशिक्षण को जब देखा जाता है तो यह प्रति प्रमासित होता है कि प्रशिक्षण, शिक्षण में निहित मंतव्यों को एकांगी रूप से पूर्ण करता है। मूलरूप से प्रशिक्षण में कार्य करना सिखाया जाता है। पढ़ाने की जिस शैली को शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को बताता है और उसे करके दिखाता है।
शिक्षार्थी अपने शिक्षक के द्वारा बतायी गई शैली के अनुरूप अनुकरण करता है और आगे चलकर उस शैली में प्रशिक्षित हो जाता है। इस प्रकार प्रशिक्षण में क्रियात्मकता होती है। इसके अन्तर्गत शिक्षार्थी द्वारा अपने बुद्धि का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता नहीं होती। प्रशिक्षण के दौरान कर्मेन्द्रियाँ अधिक क्रियाशील होती हैं। प्रशिक्षण में सीखने वालों को किसी चीज में दक्षता अभ्यास के द्वारा ही लाने का प्रयास किया जाता है। कौशल का विकास न करके प्रशिक्षण तकनीकी के विकास को मूर्त रूप देता है। प्रशिक्षण देने का कार्य विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही उपादेय होते हैं। यही कारण है कि B.Ed, B.T.C. आदि प्रशिक्षण संस्थानों में विविध प्रशिक्षणों में निष्णात व्यक्ति ही रखे जाते हैं।
निष्कर्षतः- शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मूल मान्यताओं को देखें तो शिक्षण एवं प्रशिक्षण में मूलभूत अन्तर विद्यमान है। प्रशिक्षण की शिक्षण की सापेक्ष स्थापित करने से शिक्षण के बहुआयामी स्वरूप एवं उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं होगी अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण और प्रशिक्षण दो भिन्न-भिन्न सम्प्रत्यय है।
|
|||||